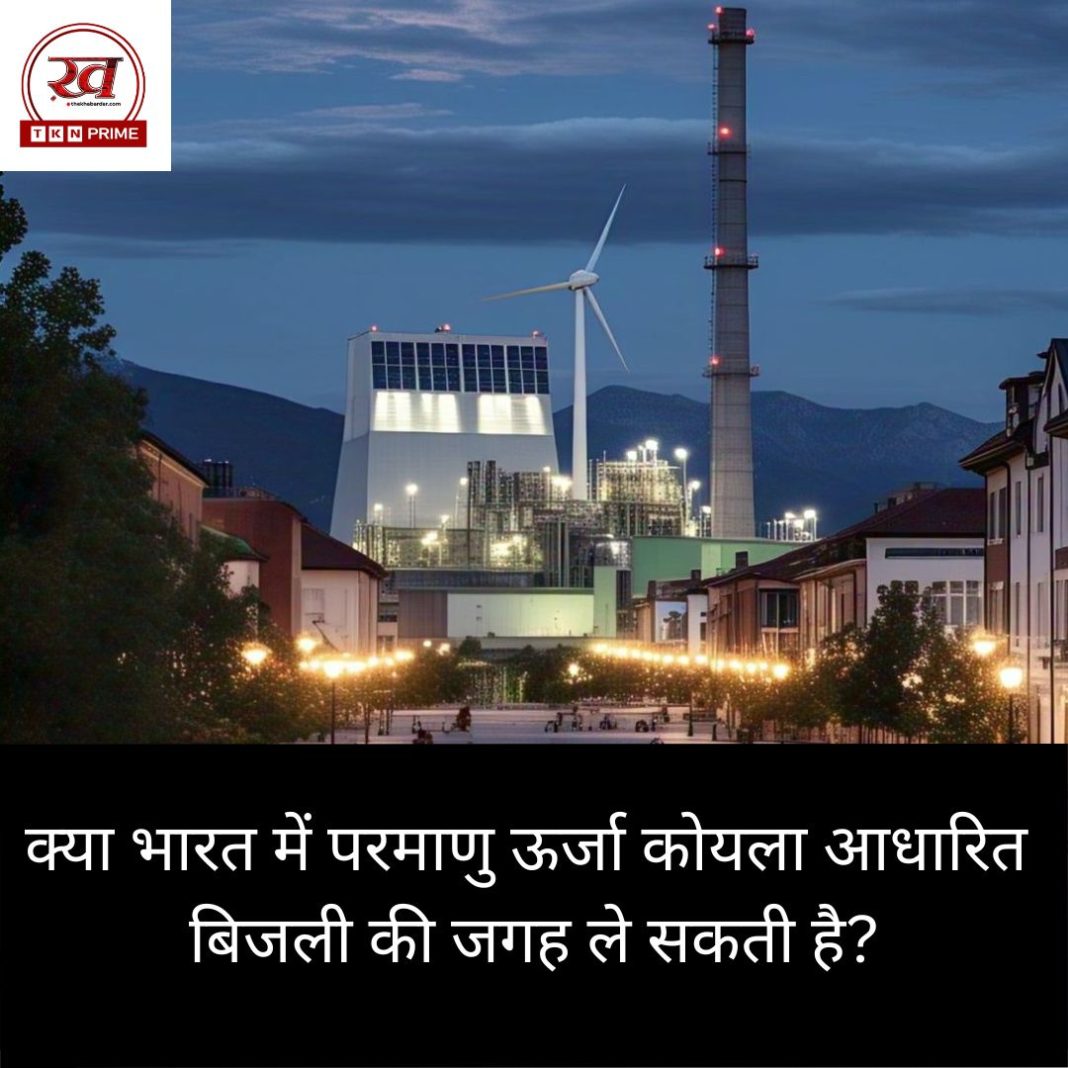भारत की ऊर्जा रणनीति कोयला, परमाणु ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों का विवेकपूर्ण मिश्रण होनी चाहिए। हालाँकि, कोयले की हिस्सेदारी कम करने की ज़रूरत है।
भारत को 24×7 स्वच्छ ऊर्जा की अपनी तेज़ी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए न्यूनतम जीवाश्म ईंधन के साथ ऊर्जा संसाधनों के इष्टतम मिश्रण की आवश्यकता है। बिजली की यह उच्च मांग आर्थिक विकास, लोगों की आकांक्षाओं और डिजिटल इंडिया पहलों के अलावा अन्य कारणों से प्रेरित है। सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट की गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है, जिसमें मुख्य ध्यान सौर और पवन ऊर्जा पर होगा।
ये दोनों संसाधन अस्थायी और परिवर्तनशील हैं। वे अकेले base load (बिजली की मांग का न्यूनतम स्तर जिसे किसी भी समय ग्रिड को लगातार आपूर्ति की जानी चाहिए ) बिजली सहायता प्रदान नहीं कर सकते हैं – और विश्वसनीयता और सुरक्षा के अपेक्षित स्तर को सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं।
ऐतिहासिक रूप से, कोयला मानव के लिए स्थिर ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत रहा है। भारत दुनिया में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। कोयला आधारित बिजली वर्तमान में इसकी 70 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करती है।
कोयले ने रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आंकड़े बताते हैं कि यह उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार देता है। खनन कार्यों से लेकर परिवहन और बिजली संयंत्र संचालन तक, कोयला रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है, खासकर झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे संसाधन संपन्न राज्यों में।
इन राज्यों के लिए कोयले को छोड़ना एक अस्तित्वगत प्रश्न है। सुपरक्रिटिकल और अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल बॉयलर जैसे तकनीकी विकास के माध्यम से संयंत्र की दक्षता में भी पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है। इसी तरह, गैसीकरण और कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस) जैसी प्रौद्योगिकियों के उद्भव के साथ पर्यावरण संबंधी चिंताओं को कुछ हद तक संबोधित किया जा रहा है।
उपरोक्त लाभों के बावजूद, कोयला तेज़ी से अपनी चमक खो रहा है। कोयला जलाना वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में अग्रणी योगदानकर्ता है, जो भारत के CO2 उत्सर्जन के 40 प्रतिशत से अधिक के लिए ज़िम्मेदार है। कोयला खनन से होने वाले वैश्विक उत्सर्जन में भारत तीसरे स्थान पर है।
इसके अतिरिक्त, कोयला खनन के कारण अक्सर पर्यावरण का क्षरण होता है, जैव विविधता नष्ट होती है और समुदायों का विस्थापन होता है। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने के लिए वैश्विक दबाव भी कोयले की दीर्घकालिक स्थिरता पर संदेह पैदा करता है।
परमाणु ऊर्जा के लाभ
कोयले की तुलना में परमाणु ऊर्जा सबसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में से एक है।
बिजली उत्पादन की प्रति इकाई जीवन चक्र CO2 उत्सर्जन 12 ग्राम है, जबकि कोयला आधारित बिजली उत्पादन के मामले में यह 820 ग्राम है।
इसके अलावा, परमाणु ऊर्जा कम मात्रा में ईंधन से उच्च ऊर्जा उत्पादन, बेस लोड समर्थन प्रदान करने की क्षमता और बड़े पैमाने पर परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा (VRE) एकीकरण के लिए एक सक्षमकर्ता के रूप में कार्य करने के लाभ प्रदान करती है। इन VRE स्रोतों में सौर, पवन, महासागर और कुछ जल विद्युत उत्पादन प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं। परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी में तकनीकी विकास के कारण परमाणु ऊर्जा संभावित रूप से लागत प्रभावी और सुरक्षित भी बन रही है।
भारत को परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी में 60 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इस अवधि के दौरान, देश ने प्रौद्योगिकी विकास, ईंधन उपयोग दक्षता और मानव संसाधन विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। परमाणु ऊर्जा विभाग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड जैसे कई संगठन इसमें योगदान दे रहे हैं।
भारतीय परमाणु संयंत्र कड़े सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं और समय-समय पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा उनकी निगरानी भी की जाती है।
भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और रूस, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अपनी परमाणु क्षमताओं को भी मजबूत किया है।
भारत चुंबकीय संलयन को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर नामक 35 सदस्यीय सहयोगात्मक प्रयास परियोजना का भी सदस्य है। द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाएँ भी बढ़ी हैं।
भारत के पास एक और लाभ यह है कि उसके पास दुनिया में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है, जो परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने का एक संभावित स्रोत है।
भारत में थोरियम-संचालित रिएक्टर हालांकि अभी तक वाणिज्यिक संचालन में नहीं हैं, लेकिन ऊर्जा स्वतंत्रता, अपशिष्ट प्रबंधन आवश्यकताओं और परमाणु प्रसार जोखिमों को कम करने की संभावना रखते हैं।
हाल के वर्षों में, जापान, अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, फ्रांस आदि सहित कई देशों में परमाणु ऊर्जा में रुचि तेजी से बढ़ी है, जो एक विश्वसनीय स्रोत और ऊर्जा क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख प्रवर्तक है। यूक्रेन युद्ध के बाद भू-राजनीतिक घटनाक्रम भी इसे बढ़ावा दे रहे हैं।
अतीत में, विनियामक अनुमोदन और निर्माण के लिए अपेक्षाकृत लंबी अवधि, निर्माण, रखरखाव और अंततः बंद करने के लिए आवश्यक उच्च पूंजी निवेश, अपशिष्ट निपटान की सुरक्षा, यूरेनियम का आयात, संभावित विकिरण और स्वास्थ्य जोखिम और ईंधन के प्रसार का जोखिम आगे बढ़ने में प्रमुख बाधाएं रहे हैं।
विवेकपूर्ण ऊर्जा मिश्रण
जबकि परमाणु ऊर्जा को तैनात करने की तकनीकी चुनौतियाँ कम होती जा रही हैं, मानव सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में आशंकाएँ एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। परमाणु संयंत्रों के लिए उपयुक्त स्थल सुरक्षित करने में अक्सर स्थानीय समुदायों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जो विस्थापन, पर्यावरणीय प्रभावों और विकिरण खतरों की संभावनाओं आदि के बारे में चिंतित हैं।
संक्षेप में, भारत की ऊर्जा रणनीति या तो एक या दूसरे विकल्प की नहीं होनी चाहिए, बल्कि कोयला, परमाणु ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों का विवेकपूर्ण मिश्रण होना चाहिए।
कोयला अपनी सामर्थ्य, प्रचुरता, रोजगार सृजन क्षमता और देश की विकासात्मक आवश्यकताओं को देखते हुए अल्पावधि में एक व्यावहारिक समाधान प्रदान करता है। हालाँकि, ऊर्जा मिश्रण में इसकी हिस्सेदारी में उत्तरोत्तर कमी आनी होगी। शुद्ध शून्य ऊर्जा परिदृश्य में परिवर्तन के लिए यह महत्वपूर्ण है।
परमाणु ऊर्जा कम कार्बन वाले भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण के साथ अधिक निकटता से मेल खाती है।
भारत परमाणु ऊर्जा विकास पर आगे बढ़ने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। इस संदर्भ में उच्च पूंजीगत लागत, सुरक्षा चिंताओं और अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है।
थोरियम रिएक्टरों की गति को तेज करना और भारत लघु रिएक्टरों और लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों जैसी स्वदेशी तकनीकों को आगे बढ़ाना ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ा सकता है और आयातित यूरेनियम पर निर्भरता को कम कर सकता है। ये छोटे रिएक्टर भारत की अच्छी तरह से विकसित प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर तकनीक के संशोधित छोटे संस्करण हैं, जो अनुकूलनीय रिएक्टरों के लिए अनुमति देते हैं, जिनका उपयोग दूरदराज के क्षेत्रों और स्टील और सीमेंट प्लांट जैसे बड़े उद्योगों के लिए किया जा सकता है। संयुक्त उद्यमों और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से इस क्षेत्र को हाल ही में खोलना इसके लिए उत्प्रेरक हो सकता है।
के रामनाथन प्रतिष्ठित फेलो हैं और अरुणेंद्र कुमार तिवारी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में एसोसिएट फेलो हैं।